नमस्कार दोस्तो , आज की हमारी इस पोस्ट में हम आपको भारत का राष्ट्रपति – President of India के संबंध में Full Detail में बताऐंगे , जो कि आपको सभी आने बाले Competitive Exams के लिये महत्वपूर्ण होगी ! पोस्ट के अंत में आपको Vice President of India से संबंधित महत्वपूर्ण Question and Answer को उपलब्ध कराएंगे, जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पुंछे जा चुके हैं व आंगे आने वाली सभी Competitive Exams के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं |
🔥 इसके अलावा Current Affairs से संबन्धित Best Course हमारी Apps पर Available है | जिसमें आपको Daily, Monthly व Yearly Current Affairs PDF व Test उपलब्ध कराते हैं | तो आप इस Course को हमारी App से खरीद सकते हैं | 🔥
इसके अलावा सभी PDF को हम अपने Apps पर व Telegram Group में भी आपको Available कराते हैं , जहां से आप इन्हें Download कर सकते हैं ! आप नीचे दी गई Link की सहायता से हमारे Apps – ” GK Trick By Nitin Gupta ” को Google Play Store से Download कर सकते हैं व Telegram Group को Join कर सकते हैं !
सभी बिषयवार Free PDF यहां से Download करें
भारत का राष्ट्रपति ( The President of India )
राष्ट्रपति, भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और यह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।
राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद – Articles related to President of India
- अनु. 52 – भारत का राष्ट्रपति
- अनु. 53 – संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनु 54 – राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल
- अनु. 55 – राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
- अनु. 56 – राष्ट्रपति की पदावधि
- अनु. 57 – पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता
- अनु. 58 – राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ
- अनु, 59 – राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
- अनु 60 – राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनु. 61 – राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- अनु. 62 – राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि ।
- अनु. 72 – क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति ।
- अनु. 73 – संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार President of India
राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of the President of india)
संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिये गए हैं। अनुच्छेद 54 में इस बात का निर्देश है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा, जबकि अनुच्देद 55 में बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी ? President of India
निर्वाचक मंडल (Electoral College)
अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा जिसमें :-
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।
इस निर्वाचक मंडल में संविधान के ”70वें संशोधन अधिनियम, 1992” के द्वारा एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया गया था। इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राज्यों की सूची में ”दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र” और ”पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र” भी शामिल होंगे।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election)
निर्वाचक मंडलके प्रावधान से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता स्वयं चुनाव द्वारा राष्ट्रपति को नहीं चुनती। संविधान सभा में इस प्रश्न पर काफी बहस भी हुई थी। अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को निम्नलिखित ठोस आधारों पर स्वीकार कर लिया गया –
- भारत की बड़ी जनसंख्या तथा वृहत आकार को देखते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करना न सिर्फ महंगा होता बल्कि समय की दृष्टि से भी अनुपयोगी होता।
- यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन कर भी लिया जाता तो समस्याएँ कम नहीं होती। शक्ति संघर्ष की संभावना बनी रहती क्योंकि पूरे देश की जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की अधीनता कभी स्वीकार न करता।
निर्वाचन की प्रक्रिया – Process of election president of india
अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया विस्तार में बताई गई है, जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा क्रमश: समझा जा सकता है –
- राष्ट्रपति के चुनावमें ‘एकल संक्रमणीय मत‘ द्वारा ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व‘ की पद्धति लागू की गई है जो मूलत: यहीं सुनिश्चित करने के लिये है कि निर्वाचित उम्मीदवार आनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक लोगों की पसंद हो। इस पद्धति में सबसे पहले एक कोटा तय कर लिया जाता है जो भारत के राष्ट्रपति के मामले में 50% से अधिक मतों का है। यह कोटा चुनाव में वास्तविक रूप से कितने मतों के बराबर होगा, यह निर्धारित करने के लिये एक फार्मूला है जो इस प्रकार है –
( डाले गये कुल मतों की संख्या / कुल स्थानों की संख्या +1 ) + 1 = कोटा
- इस पद्धति में प्रत्येक मतदाता को मत देते समय अपनी वरीयताओं का अंकन करना होता है अर्थात् उसे बताना होता है कि विभिन्न प्रत्याशियों के लिये उसकी वरीयता क्रम क्या है?
- अनुच्छेद 55(2) में बताया गया है कि सभी राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायकों के कुल मतों का योग, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग के समतुल्य बनाने के लिये कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? इस पद्धति के अनुसार सबसे पहले विभिन्न राज्यों के विधायों के मतों का मूल्य निवाला जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने का फार्मूला इस प्रकार है।
1 विधायक का मत मूल्य = (राज्य की कुल जनसंख्या)/(राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या ) × 1/1000
ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 55 (2) में संख्या की 1000 के गुणजों तक लेने की बात कही गई है और शेषफल 500 से कम हो तो उसे छोड़ देने तथा 500 से ज्यादा हो तो परिणाम में 1 जोड़ देने का निर्देश दिया जाता है ।
- इस तरह सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों के मतों का मूल्य निकाला और उन्हें जोड़ दिया जाएगा गौरतलब है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुद स्थान खाली हैं या किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो उससे राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा। President of India
- सभी राज्यों की विधासभाओं के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों के कुल योग तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल योग में समतुल्यता होनी चाहिए। इस उपबंध का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की उतनी ही भूमिका हो, जितनी केन्द्र की; ताकि हमारी राजव्यवस्था का संघात्मक ढाँचा मजबूत बना रहे।
- एक सांसद के मत का मूल्य इस प्रकार निकाला जाता है। President of India
1 सांसद का मत मूल्य = (सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य )/(संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या)
सभी विधायकों तथा सांसदों के मतों का मूल्य तय हो जाने के बाद जीतने के लिये कोटा निर्धारित किया जाता है। कोटे के अनुसार निर्धारित मत प्राप्त करने की प्रक्रिया ‘एकल संक्रमणीय’ मतों पर आधारित होती है। यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली वरीयता में कोटे के लिये अपेक्षित मत न मिले हों तो अंतिम आने वाले उम्मीदवार को पराजित घोषित कर दिया जाता है तथा उसे प्राप्त हुए प्रथम वरीयता वाले मतों का विभाजन उन मतों पर अंकित दूसरी वरीयता के अनुसार शेष प्रत्याशियों में कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटा न प्राप्त कर ले। निर्धारित कोटा प्राप्त करने के बाद उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है।
अनुच्छेद 55 में एक स्पष्टीकरण देकर बताया गया है कि विधायकों के मतों की गणना के लिये राज्य की जनसंख्या से आशय 1971 की जनसंख्या से है ‘’42वें संविधान अधिनियम 1976” के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि 2000 के बाद पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा आगे चलकर ”84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001” के माध्यम से यह स्थिति 2026 तक के लिये बढ़ा दी गई है।
राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु अर्हताएँ (Eligibilities for contesting presidential election)
अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये प्रत्याशी की अर्हताएँ बताई गई हैं। इनके अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है जो –
- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो।
- भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। इसी अनुच्छेद में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस प्रयोजन के लिये भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केन्द्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा।
राष्ट्रपति का शपथ (Oath of President of India)
राष्ट्रपति पद ग्रहरण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान होता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं –
- श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करूंगा।
- संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और
- भारत की जानता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम् न्यायालय के वरिष्ठतम् द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का निपटारा (Settlement of the disputes related to the President of india election)
अनुच्छेद 71 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जाँच तथा फैसले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये जाएंगे और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
साथ ही यह भी प्रावधान है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है तो भी उस व्यक्ति द्वारा पद धारण करने की तिथि से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि तक पद की शक्तियों के अंतर्गत किये गए कार्य अवैध नहीं होंगे।
राष्ट्रपति का निर्वाचन और संसद (The President election and the parliament)
‘राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम, 1997‘ के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिये किसी प्रत्याशी का नाम कम-से-कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तथा 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति के मामले में ये संख्याएँ 20-20 रखी गई हैं। साथ ही, इन पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिये 15 हजार रूपये की जमानत राशि निश्चित की गई है।
यदि कोई उम्मीदवार चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर लिये जाने का प्रावधान है।
राष्ट्रपति का पुनर्निवाचन (Re-election of the President)
अनुच्छेद 57 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो भी उसके पुन: इस पद के लिये चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। इस संबंध में चुनाव लड़ने के प्रयासों की कोई अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है। अर्थात् वह जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकता है। President of India
राष्ट्रपति की शक्तियाँ – Powers of the President of india
संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ विविध और व्यापक है। समझने की सुविधा के लिये इसे कुछ वर्गों में बाँटा जा सकता है –
- प्रशासनिक शक्तियाँ
- सैन्य शक्तियाँ
- राजनयिक/कूटनीतिक शक्तियाँ
- विधायी शक्तियाँ
- वित्तीय शक्तियाँ
- न्यायिक शक्तियाँ
- वीटो शक्ति
- आपातकालीन शक्तियाँ
- अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- अन्य शक्तियाँ
प्रशासनिक शक्तियां (Administrative Powers)
प्रशासनिक शक्तियों का तात्पर्य उन सभी कार्यों को करने की शक्ति से है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किये जाते हैं। अनुच्छेद 77(i) में प्रावधान है कि ”भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएगी।”
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। (अनुच्छेद 53(1)) प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें हटाने की शक्ति दी गई।
राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है –
- भारत का प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद
- भारत का महान्यायवादी
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- उच्चतम् न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
- सभी राज्यों के राज्यपाल तथा उपराज्यपाल
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य
- वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये विशेष अधिकारी
- भाषायी अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये विशेष अधिकारी आदि।
गौरतलब है कि ये सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति को अपने विवेक से नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करनी होती है। कुछ पदों के लिये वह अन्य व्यक्तियों से भी सलाह ले सकता है। जैसे – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करता है।
सैन्य शक्तियां (Military Powers)
राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति है। परन्तु, यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषण की सलाह के अनुसार कार्य करता है अनुच्छेद 74(i)।
राजनयिक / कूटनीतिक शक्तियां (Diplomatic Powers)
राजनयिक शक्तियों से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जो विदेश राज्यों के साथ संबंधों के स्तर पर लागू होती है। राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिये राजदूतों तथा कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा अन्य देशों द्वारा भारत में नियुक्त किये गए राजदूतों तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत भी करता है। President of India
विधायी शक्तियां (Legistative Powers)
भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ साथ विधायिका से जुड़ी कुछ शक्तियाँ भी रखता है जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है –
- वह संसद के दोनों सदनों को संसद सत्र हेतु आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है (अनुच्छेद 85)
- दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। (अनुच्छेद 108)
- प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। (अनुच्छेद 87) President of India
- राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित करता है जिनके पास साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। (अनुच्छेद 80) इसी प्रकार उसे यह भी अधिकार है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा के लिये नामांकित कर सकता है। (अनुच्छेद 131)
- राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह संसद के समक्ष विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत कराए। जैसे –
-
- बजट या वार्षित वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112)
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (अनुच्छेद 151)
- वित्त आयोग की अनुशंसाएँ (अनुच्छेद 281)
- संघ लोक सेवा आयोग का वार्षित प्रतिवेदन (अनुच्छेद 323)
- पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन (अनुच्छेद 340)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन (अनुच्छेद 338)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन (अनुच्छेद 338क)
- कुछ विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किये जा सकते –
- नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को परिवर्तित करने वाले विधेयक (अनुच्छेद 3)।
- धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा (अनुच्छेद 117(1))।
- ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित किये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा। (अनुच्छेद 117(3))
- ऐसा विधेयक जो उन करों के बारे में है जिनमें राज्य हितबद्ध है या जो उन सिद्धान्तों को प्रभावित करता है जिनमें राज्यों को धन वितरित किया जाता है या जो कृषि-आय की परिभाषा में परिवर्तन करता है (अनुच्छेद 274(1))
- राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणित्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं (अनुच्छेद 304)
वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)
राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ व कार्य निम्निलिखित है –
- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- वह वार्षिक वित्तीय विवरण (केन्द्रीय बजट) को संसद के समक्ष रखवाता है।
- अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है।
- वह भारत की आकस्मिक निधि से, किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है।
- वह राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बँटवारे के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है।
न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers)
- अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, परन्तु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी नहीं होती है।
- अनुच्छेद-72 के तहत राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध किये गए किसी व्यक्ति के दंड को कम करने या माफ करने की शक्ति तीन मामलों में प्राप्त होती है।
- यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है।
- यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिये दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शामिल है।
- ऐसे सभी मामले जिसमें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हो या राज्यों से। राष्ट्रपति किसी दंड के संबंध में कई तरह से क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे –
क्षमादान – क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन
- क्षमा (Pardon) : इसका अर्थ है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। इससे दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था।
- लघुकरण (Commute) : इसका अथ है किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना जैसे –
- कठोर कारावास को साधारण कारावास में;
- मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देगा।
- परिहार (Remission) : इसका अर्थ है कि आदेश बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना जैसे –
- 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना।
- विराम (Respile) : इसका अर्थ है कि दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण प्रकृति की कठोरता को कम करना। कठोरता में कमी दंड की प्रकृति बदलकर भी की जा सकती है और दंड की मात्रा कम कर के भी जैसे –
- किसी गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना।
- किसी बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास दे देना।
- प्रविलंबन (Reprieve) : इसका अर्थ है कि मृत्युदंड को अस्थाई तौर पर निलंबित कर देना, ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है, जब दोषसिद्ध अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना की होती है और राष्ट्रपति उस प्रार्थना पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में होता है।
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति – Veto Powers of the President of india
संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिये प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं (अनुच्छेद 111)
- वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है
- वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है
- वह विधेयक (धन विधेयक नहीं) को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। (हालाँकि संसद अगर इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी।)
राष्ट्रपति को यह वीटो शक्ति दो कारणों से दी जाती है।
-
- यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही हो जो संविधान के मूल भावना के विपरीत है, जो उसे रोका जा सके;
- यदि विधायिका ने कानून के कुद पक्षों पर पर्याप्त विचार-विमर्श न किया हो और ज़ल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो तो उसे सुधारा जा सके।
वीटो की यह शक्ति चार प्रकार की हो सकती है किन्तु भारतीय राष्ट्रपति के पास सामान्यत: तीन प्रकार की वीटो शक्ति है।
1. आंत्यंतिक वीटो (Absolute Veto)
इसका अर्थ है वीटो की ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित किये गए विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति को सीमित रूप से आत्यंतिक वीटो की शक्ति प्राप्त है। उदाहरण स्वरूप –
- किसी प्रायवेट सदस्य का विधेयक हो और मंत्रिपरिषद की सलाह उसके पक्ष में न हो तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है।
- यदि राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजने के बाद, किंतु उसकी अनुमति मिलने से पहले ही सरकार गिर जाए और लोकसभा के बहुमत से बनी नई सरकार अर्थात् मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को वह विधेयक अस्वीकार करने की सलाह दे, तो भी वह आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है।
2. निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto)
राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है, जब वह किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालाँकि यदि संसद उस विधेयक को पुन: किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। President of India
राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस बीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोककर रख सकता है परंतु उसे पुनर्विचार के लिये नहीं भेज सकता है।
3. जेबी वीटो (Pocket Veto)
इसका आर्थ है कि कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देना है।
राष्ट्रपति बिना कोई निर्णय किये विधेयक को अपने पास रोककर रख सकता है। इसके लिये राष्ट्रपति के पास जो वीटो सबसे प्रभावी रूप में है वह ‘जेबी वीटो’ है। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि राष्ट्रपति, संसद द्वारा पारित विधेयक को यथाशीघ्र लौटा देगा। (अनुच्छेद 111)। इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनंतकाल तक अपने पास रोककर रख सकता है।
इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण 1986 का भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक है। इस विधेयक के कुछ प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता के विरूद्ध थे। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इसके पक्ष में नहीं थे। इसलिये उन्होनें इस विधेयक पर न तो अनुमति दी, न अनुमति देने से इनकार कियाऔर न ही मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु भेजा, बस उसे अपने पास ही पड़ा रहने दिया जिससे वह कानून नहीं बन सका। President of India
4. विशेषित वीटो (Qualified Veto)
विशेषित वीटो का अर्थ ऐसी वीटो शक्ति से है जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये वीटो शक्ति नहीं है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की वीटो शक्ति है।
आपातकाली शक्तियां (Emergency Powers)
आपात उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ है –
- यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्धया बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने (या इनमें से किसी भी संभावना) के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है।
- अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या उसे समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह उस राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है।
- अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का ‘वित्तीय स्थायित्व’ या ‘साख’ संकट में है तो वह आपात् की उद्घोषणा कर सकेगा ऐसी उद्घोषणा शब्दावली में ‘वित्तीय आपात’ कहा जाता है।
- अनुच्छेद 358 में बताया गया है कि यदि आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर (सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं) की गई है, तो अनुच्छेद 19 स्वत: निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा शेष अनुच्छेदों में दिये गए मूल अधिकारों या उनमें से किन्हीं का निलंबन कर सकेगा।
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां (President’s power to promulgate ordinances)
अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि यदि संसद के दोनों- सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है तो वह अध्यादेश जारी कर सकेगा।
अध्यादेश का प्रभाव ठीक वही होता है जो कि संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। अर्थात् कहा जा सकता है कि कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी गई है कि यदि विधायिका का सत्र (संसद का सत्र) न चल रहा हो तो परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए वह स्वयं विधायिका की भूमिका में आ जाए। निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है –
- जब संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में न हो; इसका अर्थ है कि अगर एक सदन सत्र में है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है।
- अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है।
- मूल अधिकारों का उललंघन करने वाला कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता।
- अध्यादेश का जीवनकाल, सदन की बैठक से 6 सप्ताह तक रहता है। (बाद वाले सदन की बैठक से) इसी बीच-
- अगर संसद के दोनों सदन उसका अनुमोदन करने का संकल्प पारित कर दें तो वह अधिनियम बन जाता है।
- 6 सप्ताह से पहले ही दोनों सदन उसे संकल्प द्वारा खारिज कर दे तो यह समाप्त हो जाता है।
- अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता।
- राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापसले सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण विवाद इस प्रश्न पर था कि राष्ट्रपतिका यह समाधान कि अध्यादेश जारी करने के लायक परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है कि नहीं? या इसका संबंध सिर्फ राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान से है। आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ 1970 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया कि राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान को न्यायालय में इस आधारपर चुनौती दी जा सकती है कि उसने इस शक्ति का प्रयोग असद्भावपूर्ण तरीके से किया है।
अन्य शक्तियां (Other Powers)
संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति को कई अन्य शक्तियाँ भी दी गई हैं जैसे –
- अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह किसी ‘विधि’ या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है और उसे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय पर सलाह लेनी चाहिए तो वह सलाह मांग सकता है।
- हालांकि न सर्वोच्च न्यायालय अपनी सलाह देने के लिये बाध्य है और न ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए सलाह को मानने के लिये बाध्य है।
- संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है। उसे इन क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। (अनुच्देद 239) President of India
- अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें इन सूचियों में शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। (अनुच्देद 341, 342)
- राष्ट्रपति को अनुच्छेद 339 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि अनुसूचित क्षेत्रों जिसे जनजातीय आबादी के कारण विशेष संरक्षणदिया जाता है, के रूप में कुछ और क्षेत्रों को शामिल करने या कुछ क्षेत्रों को शामिल करने या कुछ क्षेत्रों को सूची से बाहर करने का निर्णय कर सकता है तथा किसी राज्य विशेष के राज्यपाल से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन मांग सकता है। इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिये बनाया गया कोई भी नियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रभावित नहीं हो सकता।
राष्ट्रपति की पदावधि – Term of the President of india
अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहरण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा उसके बाद यदि वह चाहे तो पुनर्निवाचन का प्रत्याशी हो सकता है।
5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति की पदावधि निम्न प्रकार से समाप्त हो सकती है। ये उसकी आकस्मिक मृत्यु से अलग है –
- राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपनी पदावधि समाप्त कर सकता है। (अनुच्छेद 56(1)(क))
- यदि राष्ट्रपति ‘संविधान का अतिक्रमण’ करता है तो अनुच्छेद 61 में बताई गई रीति के आधार पर उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 56(1)(ख)
- कार्यकाल समाप्त होने पर।
- यदि पद ग्रहण करने के लिए अर्ह न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो।
यदि पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने के लिये कार्यकाल चुनाव कराकर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लेना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण देरी हो तो, वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहणन कर ले।
इस स्थिति में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वाह नहीं करेगा। इसके अलावा उनकी गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।
राष्ट्रपति पर महाभियोग – Impeachment on the President of india
संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। महाभियोग एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है।
इस प्रक्रिया को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।
- सबसे पहले यदि संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर ‘संविधान के अतिक्रमण’ का आरोप लगाएगा। आरोप लगाने की कुछ शर्ते हैं –
- यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए।
- यह कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना देने के बाद प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
- सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का प्रयोजन प्रकट किया हो। President of India
- जब संसद का एक सदन ऐसा आरोप लगा देगा, तो दूसरा सदन उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा। इस अन्वेषण के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करे।
- यदि जाँच के बाद वह सदन सहमत हो जाता है कि राष्ट्रपति के विष्द्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है; और वह सदन इस संकल्प को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो ऐसा संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा।
राष्ट्रपति पद की रिक्तता तथा उसकी पूर्ति (Presidential vacanvies and their fullfillment)
जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यह रिक्ताता मृत्यु, पद-त्याग, महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से हो सकती है। President of India
क्या राष्ट्रपति ‘रबड़ की मुहर है? (Is the President a rubber stamp?)
यह सही है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषण की सलाह मानने को बाध्य है, किंतु इतने भर से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि राष्ट्रपति सिर्फ एक ‘रबड़ की मुहर’ है। वस्तुत: कई ऐसी स्थितियाँ भी हैं जिनमें राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है। जैसे –
- यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही यह निश्चय करना होता है कि स्थिर व स्वच्छ सरकार देने की दृष्टि से किसका दावा सबसे मजबूत है।
- कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विभिन्न विकल्पों पर विचार करतेहुए स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने का न्यौता देता है जो उसकी राय में लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में सक्षम हो।
- यदि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो दे तथा अविश्वास मत या विश्वास मत का सामना करने की बजाय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सलाह दे तो भी राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है।
- अनुच्छेद 74(i) में 44वें संशोधन के बाद अब राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिये लौटा सके।
- यदि लोकसभा का विघटन हो गया हो तथा नई लोकसभा का गठन न हुआ हो तो पुरानी मंत्रिपरिषद ही नई मंत्रिपरिषद के गठन तक राष्ट्रपति को सलाह देती है। इस समय राष्टप्रति को विशेष ध्यान रखना होता है कि वह किसी ऐसी सिफारिश को स्वीकार्य न करे जो चुनाव में उस दल को लाभ पहुँचाती हो या कोई बड़ा नीतिगत निर्णय करने के संबंधम में हो।
- अनुच्छेद 78 में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ बताई गई है जो राष्ट्रपति को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करती है, उदाहरण के लिये अनुच्छेद 78(ख) के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से प्रशासन तथा किसीविधान से संबंधित जानकारियाँ मांग सकता है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 78(ग) के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री को कोई विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दें, जिस पर किसीमंत्री ने विनिश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है।
अत: इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति उतना कमजोर नहीं है, जितना कुछ आलोचक बताते हैं।
भारत के राष्ट्रपतियों की सूची ( President of India List )
| क्र. | नाम | पदावधि | टिप्पणी |
| 1. | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | 1950 -1962 | राजेन्द्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, वे स्वतंत्रता सेनानीभी थे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि दो बार राष्टप्रति बने। |
| 2. | डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 1962 – 1967 | राधाकृष्णन मुख्यत: दर्शनशास्त्री और लेखक थे। आंध्रविश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। |
| 3. | जाकिर हुसैन | 1967-1969 | ज़ाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और पद्म विभूषण व भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। |
| वराहगिरि वेंकट गिरि (वी.वी. गिरि)
(कार्यवाहक) |
1969-1969 | वी.वी. गिरि पदस्थ राष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनें। | |
| 4. | मुहम्मद हिदायतुल्लाह
(कार्यवाहक) |
1969-1969 | हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा आर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। |
| वराहगिरि वेंकट गिरि (वी.वी. गिरि) | 1969-1974 | 1969 चुनाव गिरि एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति व पूर्णकालिक राष्ट्रपति दोनों बने। | |
| 5. | फख़रूद्दीन अली अहमद | 1974-1977 | फ़खद्यरूद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। |
| 6. | बसप्पा दनप्पा जत्ती (बी.डी. जत्ती)
(कार्यवाहक) |
1974-1977 | बी.डी. जत्ती, फ़ख़रूद्देीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, इससे पहले वह मैसूर के मुख्यमंत्री थे। |
| नीलम संजीव रेड्डी | 1977 – 1982 | नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्रीथे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुना गए एकमात्र सांसद थे। वे 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने। | |
| 7. | ज्ञानीजैल सिंह | 1982-1987 | जैल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृहमंत्री बनें। |
| 8. | रामास्वमी वेंकटरमन | 1987-1992 | 1942 में वेंकटरमण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद वे कॉंग्रस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा वे भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। |
| 9. | शंकरदयाल शर्मा | 1992 – 1997 | शर्मा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतके संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा वे आंध्रप्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। |
| 10. | के. आर. नारायणन | 1997-2022 | नाराश्णन जीचन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान और काकून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त भी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। |
| 11. | ऐ.पी.जे. अब्दुल कलाम | 2002 – 2007 | कलाम मुख्यत: चैज्ञानिक थे जिन्होने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया, इस कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। |
| 12. | प्रतिभा देवी सिंह पाटिल | 2007 – 2012 | प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। |
| 13. | प्रणव मुखर्जी | 2012 – 2017 | प्रणव मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेशमंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। |
| 14. | रामनाथ कोविंद | 2017 – 2022 | राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके है। |
| 15. | द्रौपदी मुर्मू | 2022 से अब तक |
भारत का राष्ट्रपति – विशिष्ट तथ्य (important facts about president of india)
- 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं।
- 1969 ई. के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी वी. वी. गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था।
- नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। President of India
- भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वी.वी. गिरि (डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण). एम. हिदायतुल्ला (वी.वी. गिरि द्वारा त्यागपत्र के कारण) एवं बी.डी. जत्ती ने (फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण) कार्य किया था।
- राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सबसे लम्बी अवधि (1950-62) तक एवं डॉ. जाकिर हुसैन ने (कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर) सबसे कम अवधि (1 वर्ष 11 दिन) तक कार्य किया था।
- संविधान सभा ने अपनी अन्तिम बैठक (14 जनवरी 1950) में निर्विरोध रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति (26 जनवरी, 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक) निर्वाचित किया था।
- डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था।
- भारतीय गणतंत्र में ( 1982 ई. में) निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे।
- डॉ. वी.वी. गिरि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। वे सबसे कम मतों के अंतर (2 प्रतिशत) से जीतने वाले राष्ट्रपति भी हैं।
- एम. हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं, जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था।
- वी.वी. गिरि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। President of India
- भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन (President House) है। 1950 ई. तक इसे वायसरॉय हाउस (Viceroy House) कहा जाता था। इसका डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन्स ने तैयार किया था।
President of India Questions and Answers in Hindi
- भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है ? – राष्ट्रपति
- राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? – राष्ट्रपति में
- भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? – राष्ट्रपति
- भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? – राष्ट्रपति
- भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? – 35 बर्ष
- राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? – अप्रत्यक्ष रूप से
- राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन-सी पद्धति अपनायी जाती है ? – समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति
- राष्ट्रपति पद के चुनाव सम्बन्धी विवाद को किसे निदेशित किया जाता है ? – उच्चतम न्यायालय को
- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम-से-कम कितनी संख्या होनी चाहिए ? – 50-50
- राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है – निर्वाचन आयोग द्वारा
- भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनायी जाती है? – राष्ट्रपति के
- राष्ट्रपति चुनाव सम्बन्धी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? – उच्चतम न्यायालय के
- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? – 5 बर्ष
- राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मण्डल में सम्मिलित होते हैं ? – स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य
- राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? –संसद के किसी भी सदन द्वारा
- राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है – महाभियोग द्वारा
- कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है ? – संसद द्वारा महाभियोग लगाकर
- राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है ? –भारत का मुख्य न्यायाधीश
- राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? – उपराष्ट्रपति को
- राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? – 6 माह में
- भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है – नीलम संजीव रेड्डी
- स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? – बिहार से
- कौन लगातार दो बार राष्ट्रपति रहे थे? –डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएँ निर्धारित करता है ? – अनुच्छेद 57
- भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी ? – डॉ. जाकिर हुसैन
- वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? – भारत के राष्ट्रपति
- किसी भी अभियुक्त की फाँसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? – राष्ट्रपति को
- लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? -14
- किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? -राष्ट्रपति को
- सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है ? –अनुच्छेद 143 के
- विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमण्डलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है ? – राष्ट्रपति
- किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया ? – एम. हिदायतुल्ला ने
- विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं ? – राष्ट्रपति
- राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता ? –धन विधेयक
- राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? – अनुच्छेद 123 के
- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरम्भ होने के कितने दिनों तक अधिक-से-अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? – 6 सप्ताह तक
- राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है ? – सर्वोच्च न्यायालय की
- राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? – 5,00,000रु.
- नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? – 15,000रु.
- भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो (Pocket Veto) शक्ति का प्रयोग किया था, वह था – भारतीय डाकघर (संशोधन) अधिनियम
- राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? – एंग्लो-इण्डियन
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा ? – सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा का पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत् पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को – अनुमति देगा
- अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन-सा अधिकार है ? – विधायी
- भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? –भारत में वंशानुगत शासन नहीं है
- एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन-सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है ? –जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है।
- भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के महासचिव भी थे ? – ज्ञानी जैल सिंह
- किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? – राष्ट्रपति को
- युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है – राष्ट्रपति
- एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है ? – कई बार
- भारतीय गणतंत्र का वह कौन-सा राष्ट्रपति था, जो सदा भारतीय धर्म-निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा ? – डॉ. एस. राधाकृष्णन
- भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष कौन है ? –राष्ट्रपति
- यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पदत्याग करने का निर्णय लेते हैं, तो वे अपना त्यागपत्र किसे सम्बोधित करके लिखेंगे ? – राष्ट्रपति को
- जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों, तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? –भारत का मुख्य न्यायाधीश
- भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है – संसद के दोनों सदनों को
ये भी पढें –
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना
- भारतीय संबिधान के मूल कर्तव्य
- राज्य के नीति-निदेशक सिद्धात
- भारतीय संविधान का संशोधन
- भारतीय संबिधान के आपातकालीन उपबंध
Join Us on Other social media
- Download Our App
- Join Our WhatsApp Group
- Join Our Telegram Channel
- Subscribe YouTube Channel
- Join Instagram
Download All PDFs in Hindi and English
- Nitin Gupta Notes PDF
- Current Affairs PDF
- Maths PDF
- Reasoning PDF
- History PDF
- Geography PDF
- Economy PDF
- Polity PDF
- Science PDF
- Computer PDF
- Environment PDF
- General Hindi PDF
- General English PDF
- Child Development and Pedagogy PDF
- UP GK PDF
- MP GK PDF
- Rajasthan GK PDF
TAG – The President of India, President of India List From 1947 to 2023, President of India GK Questions in Hindi, Rashtrapati GK in Hindi, Rashtrapati of India, Bharat ke Rashtrapati

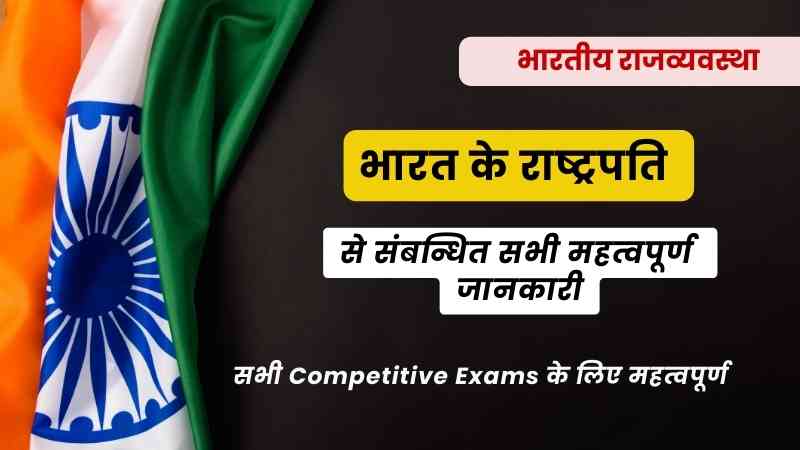


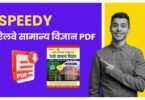




Leave a Comment