नमस्कार दोस्तो , आज की हमारी इस पोस्ट में हम आपको भारतीय संविधान का संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख संविधान संशोधन (Amendment of The Indian Constitution) के संबंध में Full Detail में बताऐंगे , जो कि आपको सभी आने बाले Competitive Exams के लिये महत्वपूर्ण होगी !
भारतीय संविधान का संशोधन
भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, इसका प्रावधान संविधान के भाग 20 (XX) के अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण आफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और इस गतिमान ब्रम्हाण्ड में कोई भी चीज सदैव गतिहीन नहीं रह सकती। कोई भी संविधान निर्मात्री सभा यह दावा नहीं कर सकती, कि उनके द्वारा निर्मित संविधान सर्वकालिक प्रकृति का सिद्ध होगा। इसका मूल कारण यह है कि हम भविष्य की सभी बातों का अनुमान लगा ही नहीं सकते और कोई भी ढॉंचा हर काल और हर परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। समय के साथ-साथ उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिये यही बात उचित है कि संविधान में ही उसके संशोधन का तरीका बता दिया जाए अन्यथा इस बात की पूरी संभावना है कि नई पीढ़ी उसे नष्ट करके अपनी आवश्यकतानुसार नया संविधान गढ़े।
सभी बिषयवार Free PDF यहां से Download करें
संशोधन की प्रक्रिया (Procedure of amendment)
किसी भी संविधान में दो तरीकों से संशोधन संभव है-
• अदृश्य या अनौपचारिक प्रक्रिया द्वारा
• दृश्य या औपचारिक प्रक्रिया द्वारा
अदृश्य या अनौपचारिक प्रक्रिया
इस प्रक्रिया में घोषित तौर पर संविधान में संशोधन नहीं किया जाता परंतु फिर भी संविधान में परिवर्तन आ जाता है। इसके मुख्यत: तीन तरीके हैं –
(क) न्यायालय द्वारा निर्वचन करके – यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय संविधान के किसी उपबंध की मौलिक व्याख्या कर दे तो वह व्याख्या ही उस प्रावधान का वास्तविक अर्थ मानी जाती है जैसे- विभिन्न लोकहित वादों में संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या में बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हैं जो मूल संविधान में नहीं थी।.
RRB NTPC 2024-25 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी APP पर उपलब्ध " RRB NTPC 2024 - Best PDF Notes and Test Series" को Join कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा -
- All Subjects Best PDF (GK, Current Affairs, Maths and Reasoning)
- Previous Year Paper PDF
- Test Series Subjectwise
- Full Test
- सभी PDF को Mobile में Download करने की सुविधा
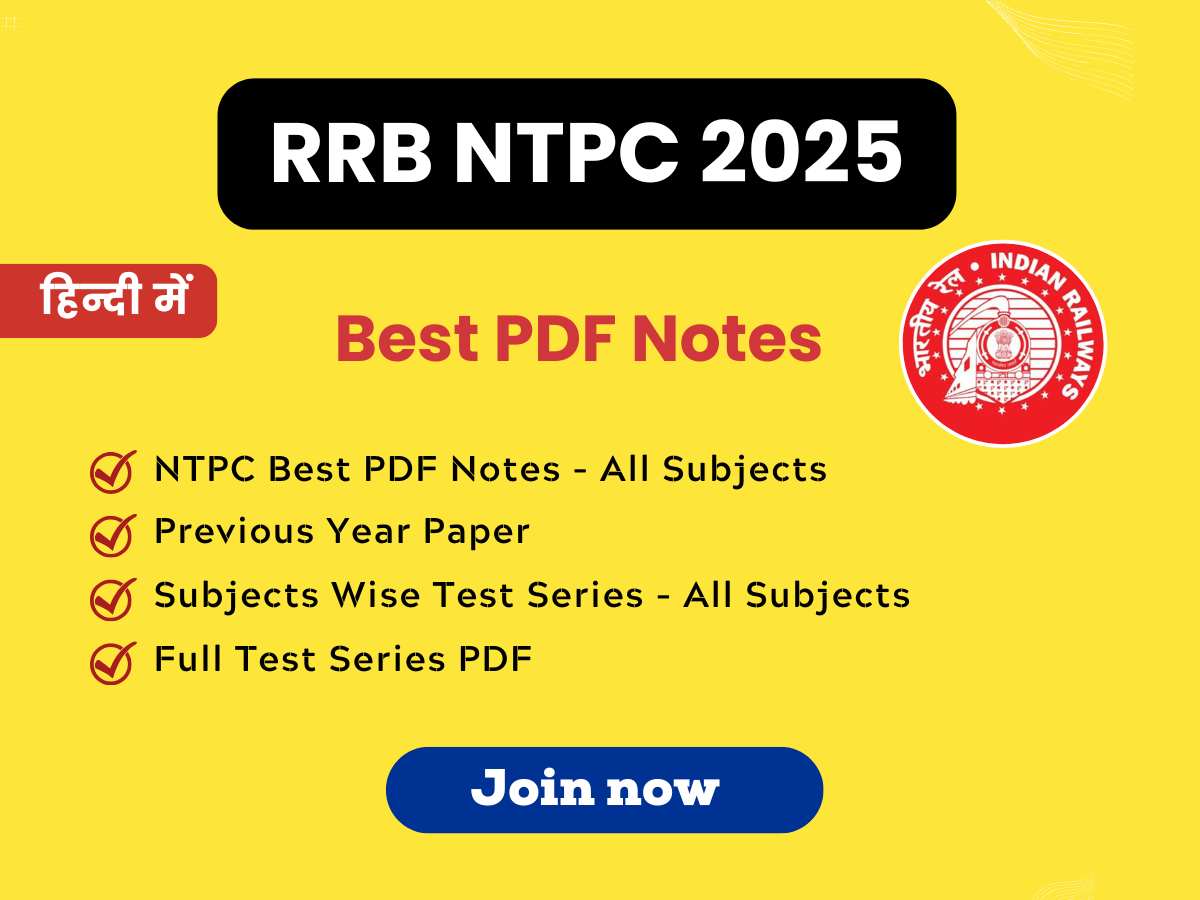
Best PDF Notes के लिए हमारी App पर सबसे ज्यादा Popular Course
आप सभी हमारी APP पर उपलब्ध Best Course को Join कर सकते हैं - जिसमें बहुत ही कम दाम में आपको Best PDF Notes उपलब्ध कराये गए हैं
| Best PDF Notes in Hindi - All Subjects | Join Now |
| Best PDF Notes in English - All Subjects | Join Now |
| GK Trick by Nitin Gupta - सामान्य ज्ञान and करेंट अफेयर्स का Solutions | Join Now |
| Current Affairs 2024-25 Course By Nitin Gupta - करेंट अफेयर्स का Solutions | Join Now |
| RRB NTPC 2025 - Best PDF Notes and Test Series | Join Now |
| RRB Group D 2025 - Best PDF Notes and Test Series | Join Now |
(ख) अभिसमय अर्थात् संवैधानिक परंपराओं के पालन द्वारा – राष्ट्रपति की जेबी वीटो या ‘पाकेट वीटो’ राष्ट्रपति- मंत्रिपरिषद संबंध, बहुमत स्पष्ट न होने पर राष्ट्रपति द्वारा सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करना आदि अभिसमय के ही उदाहरण हैं।
(ग) विधायन द्वारा आपूर्ति करके – जैसे – नागरिकता अधिनियम, 1955 आदि।
दृश्य या औपचारिक प्रक्रिया
इस प्रक्रिया में संविधान में बताए गए तरीके से संशोधन होता है। यह परिवर्तन की घोषित और प्रकट प्रक्रिया है। भारत के संविधान में यह तीन तरीके से संभव है-
(क) कुछ उपबंधों में साधारण बहुमत द्वारा
(ख) कुछ उपबंधों में विशेष बहुमत द्वारा
(ग) कुछ उपबंधों में विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन
(क) साधारण बहुमत द्वारा संशोधन
संविधान के जिन उपबंधों का विशेष संवैधानिक महत्व नहंी है उनमें संशोधन करने के लिये अत्यन्त लचीली प्रक्रिया अपनाई गई है। ध्यातव्य है कि इन उपबंधों में संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। ये उपबंध दो प्रकार के हैं-
- जहाँ संविधान का पाठ नहीं बदलता परंतु विधि में परिवर्तन आ जाता है– जैसे अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को है परंतु अनुच्छेद 5 से 10 तक के अनुच्छेद वैसी ही लिखे रहेंगे। अनुच्छेद 124 में आज भी लिखा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और सात से अनधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जबकि संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 30 कर दी है।
- जहां संविधान का पाठ परिवर्तित हो जाता है– इनमें से कुछ प्रमुख उपबंध निम्न हैं-
- नए राज्य का निर्माण या विद्यमान राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन
- पहली, चौथी, पॉंचवी, छठी अनुसूची के विषय
- विधान परिषद का सृजन या उत्सादन
- संघ राज्यक्षेत्रों के लिये विधानमण्डल या मंत्रिपरिषद या दों का सृजन
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों, कुछ अन्य संवैधानिक पदों के वेतन-भत्ते आदि।
- संसदीय विशेषाधिकार का निर्धारण
- अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी के प्रयोग का 15 वर्ष से अधिक के लिये विस्तार
- दूसरी अनुसूची से संबंधित कुछ अनुच्छेद (75, 97, 125, 148 आदि)
(ख) विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
जो उपबंध ‘साधारण बहुमत द्वारा संशोधन’ और भारत के संघ्ज्ञीय ढॉंचे से संबंधित उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं उन सभी में विशेष बहुमत से संशोधन होता है। विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि ऐसे संशोधन विधेयक को-
- प्रत्येक सदन में ‘उपस्थित और मतदान करने वाले’ सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई (2/3) का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। ‘उपस्थित तथा मतदान करने वाले’ सदस्यों का अर्थ है कि यदि कुछ सदस्य मतविभाजन के समय उपस्थित हों परन्तु मतदान में हिस्सा न लें तो दो-तिहाई की गणना के लिये उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। स्पष्टत: (2/3) की गणना में उसी की गिनती होगी जो न केवल उपस्थित हो बल्कि मतदान में भी भाग ले।
- सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिये। सदन की कुल संख्या का अर्थ सदन की समस्त संख्या से है न कि उस समय मौजूद सदस्यों की संख्या से।
(ग) विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन
संविधान के वे प्रावधान जो संघात्मक संरचना से संबंधित हैं उनमें संशोधन कठोर है तथा उनमें संशोधन तभी संभव है जब संसद के दोनों सदनों से विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाए और उसके पश्चात कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का ‘संकल्प’ पारित करके उसे अनुसमर्थन दिया जाए। ये उपबंध निम्न हैं। जैसे- अनुच्छेद-54, 35, 73, 162, 241 आदि में किया जाने वाला संशोधन।
- राष्ट्रपति निर्णाचन से संबंधित उपबंध
- संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित उपबंध
- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित उपबंध
- संसद में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित विषय
- संघ और राज्य के विधायी शक्तियों से संबंधित विषय
- अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्न हैं-
- संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पुर:स्थापित किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि इसके लिये राष्ट्रपति की सिफारिश/पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिये।
- विशेष बहुमत की शर्त सभी प्रक्रमों पर लागू होती है जैसे-विधेयक पर विचार, विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाना, मूल विधेयक में सेशोधन तथा विधेयक पारित किया जाना आदि।
- विशेष स्थिति में विधेयक को आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा।
- यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच विधेयक को लेकर किसी प्रकार की असहमति है तो संयुक्त बैठक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
- पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जाएगा। इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की कोई वीटो पावर प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिये बाध्य है अर्थात् उसे हर हालात में इस विधेयक को अपनी अनुमति देनी ही होगी।
आधारभूत ढॉंचा (Basic structure)
- कुछ देशों के संविधान में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि किन-किन उपबंधों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के उपबंधों को सुरक्षित या असंशोधनीय उपपबंध कहते हैं।
- संविधान संशोधन की शक्ति पर जो मर्यादायें संविधान मंे ही निर्दिष्ट कर दी जाती हैं उन्हें अभिव्यक्त मर्यादायें कहते हैं। कुछ संविधानों में ये मर्यादायें नहीं बतायी जाती अपितु ये मर्यादायें न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं, इन्हें ‘विवक्षित मर्यादायें’ कहते हैं।
- भारतीय संविधान के जो आधारभूत लक्षण निर्धारित किये गए हैं, वह एक विवक्षित मर्यादा है क्योंकि संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सवौच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में, जिनमें से ‘केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य’ प्रमुख हैं, यह बताया है कि संविधान के आधारभूत ढॉंचे में कौन-कौन से तत्व उपस्थित हैं। यह सूची अंतिम नहीं है अपितु न्यायालय समय-समय पर इस सूची में तत्वों को शामिल करता रहा है और आगे भी कर सकता है।
- ‘एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)’ में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता (धर्मनिरपेक्षता) को न केवल आधारभूत ढॉंचे का तत्तव माना अपितु धर्मनिरपेक्षता (पंथनिरपेक्षता) की व्याख्या भी की।
- ‘मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले’ में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ को आधारभूत ढॉंचे का अंग माना।
- उच्चतम न्यायालय ने अब तक निम्नलिखित तत्वों को संविधान के आधारभूत ढॉंचे में शामिल किया है-
o विधिसम्मत शासन (रूल ऑफ लॉ)
o संविधान की सर्वोच्चता
o राजव्यवस्था का प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र होना
o शक्तियों का पृथक्करण का सिंद्धांत
o शासन की संसदीय प्रणाली
o न्यायपालिका की स्वतंत्रता व न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति
o संसद की संविधान का संशोधन करने की सीमित शक्ति
o समता का सिद्धांत
o संविधान का संघात्मक ढॉंचा
o स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन
o सामाजिक व आर्थिक न्याय का उद्देश्य
o राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप
o मूल अधिकार व नीति-निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन
o मूल अधिकारों का सार (यद्यपि मूल अधिकरों में संशोधन हो सकता है)
संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति (Power of parliament to amend the consitution)
संविधान के आधारभूत लक्षणों की स्थापना के पश्चात् यह तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, वह असीमित नहीं है। वर्तमान समय में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति इस प्रकार है-
- संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है परंतु यह शक्ति आधारभूत ढॉंचे की ‘विवक्षित परिसीमा’ से बँधी हुई है। न्यायालय को यह तय करने की शक्ति है कि संसद द्वारा किया गया संशोधन संविधान के ‘आधरभूत ढाँचे’ के विरूद्ध है या नहीं।
- संविधान संशोधन की वैधता का परीक्षण अनुच्छेद 13 के संदर्भ में नहीं किया जा सकता।
- संसद, संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 में दी गई अपनी शक्ति को बढ़ा नहीं सकती क्योंकि ‘संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति’ आधारभूत ढॉंचे का तत्व है।
- आधारभूत ढॉंचे के आधर पर न्यायालय उन्हीं संशोधनों को खारिज कर सकता है जो 24 अपैल, 1973 (केशवानंद भारती की निर्णय तिथि) के बाद पारित किये गए हों।
- किसी विशय को यदि संसद 9वी अनुसूची में 24 अप्रैल, 1973 के बाद शामिल करती है तो उस पर इस आधार पर आक्षेप हो सकेगा कि वह आधारभूत ढॉंचे के विपरीत है।
- संशोधन के लिये जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह आवश्यक है। यदि उसका पालन न किया गया तो संशोधन अविधिमान्य हो जाएगा।
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिये यदि संविधान का संशाधन किया जाता है तो उससे आधारभूत ढॉंचे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- इस संपूर्ण स्थिति में परिवर्तन तभी संभव है जब 13 या 13 से अधिक न्यायाधीशों की कोई न्यायपीठ केशवानंद भारती मामले का निर्णय पलट दे और आधारभूत ढॉंचे के सिद्धांत को अवैध घोषित कर दे।
प्रमुख संविधान संशोधन (Major constitutional amendments)
1. 7वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 1956– इसके द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों की मॉंग का समाधान करने के लिये ‘राज्य पुनर्गठन आयेग’ की रिपोर्ट को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया और पूरे भारत को 14 राज्यों व 6 संघ राज्य-क्षेत्रों में बॉंट दिया गया।
2. 24वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 1971– इसके द्वारा यह नियम बना दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिये बाध्य है।
3. 42वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 1976– यह संशोधन मुख्यत: सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का मूर्त रूप था। यह व्यापक संविधान संशोधन है और कई कारणों से चर्चित एवं विवादित रहा। इसके माध्यम से कुल 53 अनुच्छेद और सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गए। इसके माध्यम से संविधान का व्यापक पुनरीक्षण किया गया और कई आधारभूत महत्व के उपबंधों को बदला गया। इन्हीं कारणां से इस संविधान संशोधन को ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-
• संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता शब्द जोड़े गए।
• संविधान में अनुच्छेद 51(क) अंत:स्थापित कर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए।
• लोकसभा और विधानसभाओं की समयावधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।
• अनुच्छेद 74 को संशोधित करके यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
• यह निर्धारित किया गया कि यदि संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन करती है तो उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधर पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।
• राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के आधार पर भारत के किसी क्षेत्र विशेष के लिये भी ‘आपात की उद्घोषणा’ कर सकता है।
• सातवीं सनुसूची में संशोधन कर ‘राज्य सूची’ में कुछ नई प्रविष्टियॉं शामिल की गई तथा ‘राज्य सूची’ की कुछ प्रविष्टियों को जैसे – शिक्षा, नाप-तौल, वन आदि को ‘समवर्ती सूची’ का विषय बनाया गया।
4. 44वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 1978– इसका वास्तविक उद्देश्य 42वे संशोधन द्वारा संविधान मे ंकिये गए व्यापक परिवर्तनों को निरसित कर संविधान को उसके मूल स्वरूप में लाना था। इसके द्वारा किये गए परिवर्तनों में से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं-
• संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकरा की जगह कानूनी अधिकार बना दिया गया।
• अनुच्छेद 71 को संशोधित कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की जॉंच का अधिकार पुन: सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया। (39वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा यह अधिकार छीन लिया गया था)
• राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद को उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिये कह सकेगा और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने को बाध्य होगा।
• लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को पुन: 5 वर्ष कर दिया गया।
• न्यायालय को उसकी कुछ शक्तियॉं पुन: प्रदान की गई।
• इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत ‘आपात की उद्घोषणा’ में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए-
(क) ‘आंतरिक अशांति’ के स्थान पर ‘सशस्त्र’ विद्रोह को आधर बनाया गया।
(ख) आपात की उद्घोषणा के लिये मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया।
(ग) उद्घोषणा को 2 माह और सामान्य बहुमत के बजाय 1 माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद से पारित होना अनिवार्य किया गया। साथ ही हर 6 माह बाद पुन: अनुमोदन को अनिवार्य बनाया गया।
5. 52वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 1985– इसके द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची शामिल करके ‘दल-बदल कानून’ को मान्यता प्रदान की गई।
6. 61वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 1989- साधारण चुनावों में मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
7. 69वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 1991– संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन के अंतर्गत दिल्ली में मंत्रियों की संख्या 10% कर दी गई।
8. 73वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 1992– संविधान में 11वी अनुसूची शामिल किया गया और पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
9. 74वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 1992– संविधान में भाग 9(क) और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा नगर निकायों को शासन की स्वायत्त इकाई के रूप में मान्यता दी गई।
10. 86वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 2002– प्राथमिक शिक्षा से जुड़े इस संशोधन विधेयक द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किये गए-
(क) संविधान में एक नया अनुच्छेद 21(क) को स्थापित करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये ‘नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा’ को मूल अधिकार बना दिया गया।
(ख) अनुच्छेद 45 में संशोधन करके यह लियाा गया कि- राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे छ: वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रयास करेगा।
(ग) मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 क में 11वॉं मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें बताया गया कि, ”माता-पिता और संरक्षक अपने 6-14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिये यथासंभव शिक्षा प्राप्त कराएंगे।”
11. 89वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 2003– इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338(क) अंत:स्थापित करके ‘अनुसूचित जनजातियों’ के लिये राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
12. 91वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 2003– इस संशोधन के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-
(क) मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या (प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित), लोकसभा या विधानसभा क समस्त सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
(ख) किसी दल का अन्य दल में विलय तभी मान्य है जब उसके कम से कम दो तिहाई (2/3) सदस्य यह निर्णय लेते हैं।
(ग) दल-बदल करने वाला कोई भी व्यक्ति मंत्री या सवेतन राजनीतिक पद धारण करने के योग्य नहीं रहेगा। यह निरर्हता तब तक बनी रहेगी जब तक सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती हया वह किसी सदन के लिये निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता था वह किसी सदन के लिये निर्वाचन में भाग नहीं लेता, इनमें से जो भी पहले हो।
13. 92वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 2003– इसके द्वारा आठवीं अनुसूची में 4 और भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार अब आठवीं अनुसूची में 22 भाषाऍं हैं।
14. 97वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 2011– इसके द्वारा संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किये गए-
(क) संविधान में भाग 9(ख) सहकारी समितियॉं जोड़ा गया। इसमें सहकारी समितियों के गठन, विनिमयन, विघटन से संबंधित उपबंध है।
(ख) नीति-निर्देशक तत्वों (भाग-4) के अंतर्गत अनुच्छेद 43(ख) जोड़ा गया जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करने का निर्देष देता है।
(ग) अनुच्छेद 19(1)(ग) के अंतर्गत संघ बनाने के साथ-साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार मूल अधिकार माना गया।
15. 100वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 2015– इसके तहत कुछ क्षेत्र का भारत और बांग्नादेश के मध्य आदान-प्रदान हुआ और बांग्लादेश के जो हिस्से भारत में आए उनमें रहने वालों की भारतीय नागरिकता दी गई।
16. 101वॉं संविधान संशोधन अधिनियम, 2016- इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 279क के अनुसार जीएसटी काउंसिल का गठन हो जुका है। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 366, 368 में संशोधन किया गया। छठी अनुसूची एवं सातवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया।
परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
- भारत के संविधान में संशोधन की शुरूआत लोकसभा या राज्यसभा द्वारा की जाती है।
- संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन राज्य विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है।
- भारतीय संविधान में महला संशोधन 1951 में हुआ था। यह संशोधन भूमि सुधार विधियों से संबंधित था। इस संशोधन द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।
- 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के पश्चात् राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिये बाध्य है।
- सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति को सीमित किया।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम ‘भविष्यलक्षी विनिर्णय’ के सिद्धांत को लागू किया।
- केशवानंद भारती वाद (मामले) की सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायमूर्ति श्री सीकरी ने की थी।
- 97वॉं संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियों से संबंधित है।
- 86वॉं संविधान संशोधन 2002, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती के मामले में आधारभूत ढॉंचे के सित्रांत का प्रतिपादन किया।
- संविधान का संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति संविधान का आधारभूत लक्षण है।
- अमेरिका, आस्ट्रेलिया और स्विटजरलैण्ड के संविधान कठोर स्वरूप के हैं।
- उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में साधारण बहुमत से संशोधन संभव नहीं है।
ये भी पढें –
Click Here to Subscribe Our Youtube Channel
दोस्तो आप मुझे ( नितिन गुप्ता ) को Facebook पर Follow कर सकते है ! दोस्तो अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इस Facebook पर Share अवश्य करें ! क्रपया कमेंट के माध्यम से बताऐं के ये पोस्ट आपको कैसी लगी आपके सुझावों का भी स्वागत रहेगा Thanks !
दोस्तो कोचिंग संस्थान के बिना अपने दम पर Self Studies करें और महत्वपूर्ण पुस्तको का अध्ययन करें , हम आपको Civil Services के लिये महत्वपूर्ण पुस्तकों की सुची उपलब्ध करा रहे है –
UPSC/IAS व अन्य State PSC की परीक्षाओं हेतु Toppers द्वारा सुझाई गई महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची
Top Motivational Books In Hindi – जो आपकी जिंदगी बदल देंगी
TAG – Amendment of The Indian Constitution , भारतीय संविधान का संशोधन , samvidhan me sanshodhan ki prakriya , bhartiya samvidhan me sanshodhan

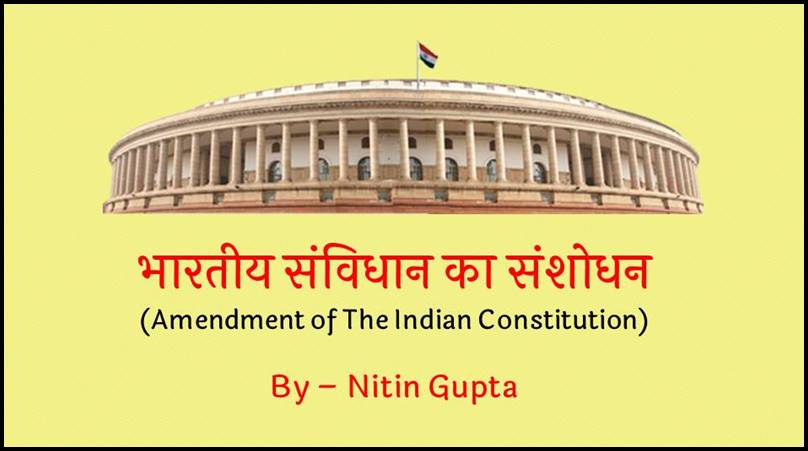




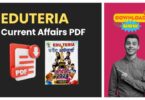
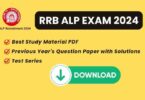



बहुत अच्छा